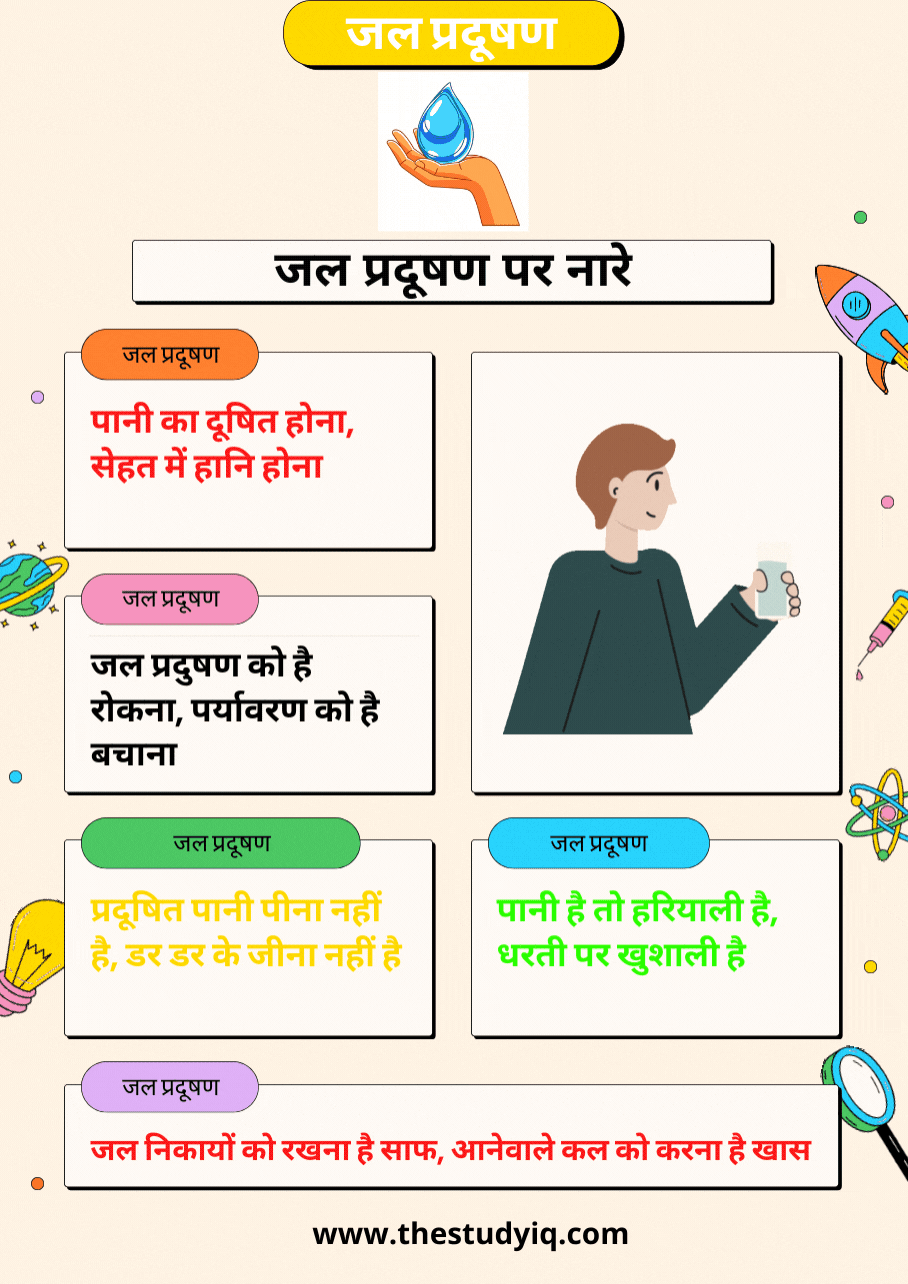जल प्रदूषण (Water Pollution)
जल प्रदूषण का चित्र
जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में जल प्रदूषण की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से दी गयी है-
"जल प्रदूषण से तात्पर्य जल के ऐसे संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसे परिवर्तन या जल में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मल-मूत्र या व्यावसायिक निःस्त्राव या किसी अन्य द्रव या ठोस पदार्थ के उत्सर्जन से है, जो लोक संकट उत्पन्न करे या कर सके या जो ऐसे जल का सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए या जलीय जीवों के जीवन या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या क्षतिकर हों। jal pradushan kya hai जल प्रदूषण इन हिंदी
जल प्रदूषण के स्त्रोत (Sources of Water Pollution)
सामान्य जल प्रदूषण के दो स्त्रोत हैं। jal pradushan ke karan
- प्राकृतिक स्त्रोत (Natural Sources)
- मानवीय स्त्रोत (Human Sources)
1. प्राकृतिक स्त्रोत (Natural Sources)
प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल में भी अशुद्धि होती है। प्राकृतिक रूप से जल में प्रदूषण धीमी गति से होता रहता है। प्राकृतिक स्त्रोतों का जल जहां बहकर आता है या जहां एकत्रित होता है, वहां यदि खनिजों की मात्रा अधिक होती है तो वे खनिज पानी में मिल जाते हैं। इनकी मात्रा में वृद्धि हो जाने से जल प्रदूषित हो जाता है।
भूमि की सतह से बहकर गया हुआ जलः सतह से बहकर गए हुए प्रदूषक (चक्रवाती जल) भूमि की प्रकृति पर निर्भर करते है जिससे बहकर यह आया है। कृषि भूमि से बहकर आए जल कीटनाशक अवशेषों तथा क्षेत्र से बहकर आए जल का जैविक अपघटन हो जाता है क्योंकि ये कार्बनिक प्रदूषक को उत्पन्न करते है। औद्योगिक स्थलों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषक जैसे भारी धातु होता है। ये सभी प्रदूषक बहकर हमारे सतह जल तथा जल स्रोत को भारी मात्रा में संक्रमित करते है।
जल प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारक मानवीय स्त्रोत हैं। इन स्त्रोतों में प्रमुख निम्न है-
- औद्योगिक अपशिष्ट : बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां छोटे-छोटे कल-कारखाने, नदियों के जल का अधिकाधिक प्रयोग करके अपशिष्टों को पुनः नदियों नालों में डालकर जल को प्रदूषित करते हैं। फलस्वरूप सभी नदियां दूषित हो चली हैं। लखनऊ में गोमती का जल कागज और लुग्दी के कारखानों से निकले अवशिष्टों से दुषित होता है। तो दिल्ली में यमुना का जल डी.डी.टी. के कारखानों से निकाले पदार्थों से प्रदूषित होता है। लघु तथा बड़ी औद्योगिक क्रियाओं द्वारा गंदेजल का उत्पादन होता है, जो विविध प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक प्रदूषकों द्वारा संक्रमित होते है। भारत की लगभग सभी नदियां कम से कम 4 खास जगहों पर औद्योगिक गंदे जल के द्वारा अधिक प्रदूषित है। यहां तक कि समुद्री पर्यावरण भी अछूता नहीं है, ज्यादातर तटीय जल को तटीय उत्सर्जन झींगा संवर्धन फॉर्म तथा मछली प्रसंस्करण उद्योग से खतरा है। औद्योगिक उत्सर्जन के ज्यादातर अवयव कम सांद्रता होने पर भी पारितंत्र के लिए जहरीले है तथा बहुत से अवयवों का जैविक अपघटन संभव नहीं है। गर्म जल दूसरा प्रमुख औद्योगिक प्रदूषक है। बहुत से उद्योगों जैसे ऊर्जा संयंत्र तथा तेल संशोधकों में जल का उपयोग मशीन को ठंडा करने के लिए होता है। गर्म गंदे जल का उत्सर्जन जिसका तापमान लिए गए जल से अधिक होता है। अतः इससे जल तंत्र में ताप प्रदूषण हो जाता है।
- नगरीय गंदे जल : घरेलू क्रियाओं, रसोई, पैखाने एवं अन्य घरेलू जल तरल गंदे जल के रूप में बाहर आते है। ज्यादातर ये नदियों में सीधे गिरा दिए जाते है या किसी नजदीक के जल तंत्र में डाल दिए जाते है। कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील भी घरेलू सीवेज के डालने से पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। घरेलू उत्सर्जक ज्यादातर कार्बनिक मल-मूत्र ढोती है जिसका जैव अपघटन संभव है। ज्यादातर पोषक धुलाई के अवशेष से आते है जैसे फॉस्फेट तथा कार्बनिक अवशेष (जैसे नाइट्रेट)।
- कृषि पदार्थ : उर्वरक तथा कीटनाशक पदार्थों को खेतों में डालने से फसलों द्वारा कुछ मात्रा के प्रयोग कर लिए जाने के पश्चात् इनका अधिकांश भाग वर्षा के जल द्वारा बहकर नदी, नालों में मिल जाता है। और जल को दूषित करता है।
- नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग : नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से वातावरण में असंख्य रेडियोधर्मी कण उत्पन्न हो जाते हैं। जो वर्षा का जल में घुलकर जल को प्रदूषित करते है।
- फ्लाई ऐश : देश में पर्याप्त मात्रा में ताप विद्युतघर हैं। जिनसे प्रतिदिन हजारों टन राख उत्पन्न होती है जो वर्षों तक जमीन पर पड़ी रहती है अथवा वर्षा के माध्यम से तालाबों एवं नदियों तक पहुंचती है। इस फ्लाई ऐश में लगभग सभी भारी धातुएं विद्यामान रहती है। जो धीरे-धीरे भूमि के अन्दर प्रवेश करती हैं। जिससे इनके आसपास के क्षेत्र का भूमिगत जल तथा सतही जल विषाक्त हो जाता है।
- ईंधनों का जलना : पेट्रोलियम, खनिज, कोयला तथा अन्य ईंधनों के जलने से वायु में सल्फर डाइऑक्साइ, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा अन्य गैसें वर्षा के जल में घुलकर अम्ल तथा अन्य लवण बनाकर जल को प्रदूषित करते हैं।
- तेल अधिप्लाव : तेल अधिप्लाव सागर में पेट्रोलियम के दुर्घटना से गिरने के कारण होता है। तेल टैंकर के उलटने, तटीय इलाके में तेल का खनन, तेल खोज ऑपरेशन तथा तेल शोधकों के द्वारा जलीय पारिस्थितिक तंत्र तेल आवरण से तटीय क्षेत्र की सुंदरता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्लावक मछलियों तथा समुद्रीय चिड़ियों की मृत्यु हो जाती है। इससे पारिस्थितिक तंत्र पर तेल अधिप्लाव का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तेल अधिप्लाव का प्रवाल भित्ति पर भी बुरा असर पड़ता है तथा ये स्थानीय जलीय जैव विविधताओं को बहुत हद तक नुकसान पहुँचा सकते है।
- डिटर्जेण्ट्स तथा साबुन : नहाने धोने, कपड़ा साफ करने में डिटर्जेण्ट्स साबुन का प्रयोग किया जाता है। इससे जल प्रदूषित होता है।
- सीबेज : मल-मूत्र कूड़ा-करकट आदि नदियों, तालाबों झीलों में छोड़ जाने से जल प्रदूषण बढ़ता है।
जल प्रदूषक हो सकते है
- जैविक (रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल, हैलमैथिस)
- रासायनिक (कार्बनिक रासायनिक जैसे जैवनाशंक पॉलीक्लोरीनेटेड बाईफिनायल या PCB, अकार्बनिक रासायनिक,जैसे फॉस्फोट नाइट्रेट, फ्लोराइड इत्यादि तथा भारी तत्व जैसे As, Pb, Cd, Hg इत्यादि)
- भौतिक (उद्योगों से निकले गर्म जल तेल वाहक से गिरा हुआ तेल) प्रदूषक विभिन्न स्रोतों तथा क्रियाओं से पैदा होते है, जिसकी संक्षिप्त में निम्नलिखित व्याख्या दी गई है।
जल प्रदूषण के प्रभाव (Effects of Water Pollution)
जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव (Effects on Aquatic Ecosystem)
जल प्रदूषण से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अभिलक्षणों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
- बीमारियां: प्रदूषित जल के प्रयोग से नाना प्रकृति के रोगों की संभावना बनी रहती है। यथा-पक्षाघात, पोलियों, मियादी बुखार हैजा डायरिया, क्षयरोग, पेचिश, इसेफलाइटिस, कनजक्टीवाइटिस, जांडिस, आदि रोग फैल जाते है। फसलों पर प्रभावः प्रदूषित जल से सिचाई करने से फसलें खराब हो जाती हैं। इन फसलों, फूलो, सब्जियों आदि के प्रयोग से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।
- जलीय जीवों की हानि: जलीय जीव विष तथा अन्य प्रदूषकों को केवल न्यून मात्रा में ही सहन कर सकते हैं अन्यथा ये प्रदूषक इनके लिए घातक होते हैं। कुछ जीवों तथा मछलियों पर इसका प्रभाव शीघ्र पड़ता है।
- पर्यावरणीय कारकों का प्रभावः जल के पी. एच. मान, ऑक्सीजन तथा कैल्शियम की मात्रा पर जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, जस्ता तथा सीसा के प्रदूषित जल प्रायः जैव-सृष्टि से शून्य हो जाते हैं।
- शैवालों को हानिः निलंबित कणों के नदियों, तालाबों आदि के नाली में बैठने से वहां के शैवाल एवं अन्य जलीय पौधे समाप्त हो जाते है।
- अन्य प्रभाव: जल प्रदूषण के उपरोक्त प्रभावों के अतिरिक्त कुछ अन्य दुष्प्रभाव होते है, प्रदूषित जल से निर्मल जल के स्त्रोत नष्ट हो जाते हैं, अम्लीय प्रदूषक तत्वों की उपस्थित वाले जल से धातु निर्मित नलों व टंकियों में संक्षरण होता है, प्रदूषित जल जैसे सीवेज के विघटन से ज्वलनशील गैंसे उत्पन्न होती हैं, प्रदूषित जल सिंचाई के लिए हानिकारक होता है, प्रदूषित जल के शोधन पर सरकार व गैर-सरकारी संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों को बहुत खर्च उठाना पड़ता है। प्रदूषित पदार्थों के आधिक्य के कारण जल में घुली हुई ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen: DO) की मात्रा घट जाती है, जिससे कुछ संवेदी जीवों जैसे प्लवक, मोलस्क एवं कुछ मछलियों की मृत्यु हो जाती है। मात्र कुछ सहनशील प्रजातियाँ जैसे एनेलीड तथा कुछ कीट ही कम DO में जीवित रह पाते हैं। ऐसे जीवों को प्रदूषित जल की सूचक प्रजातियों (Indicator Species) के रूप में पहचाना जाता है। जैवनाशक (Biocides), पॉली क्लोरीनेटेड बाईफिनाइल्स (PCBs) और भारी धातुएँ, जैसे- पारा, सीसा, कैडमियम, तांबा, चांदी आदि, जीवों की विभिन्न प्रजातियों को सीधे ही नष्ट कर देती है उच्च तापमान पर जल में ऑक्सीजन का विलयन कम होता है। अत: उद्योगों से निकले अपशिष्ट गर्म जल को जब जलाशयों में डाला जाता है तो वह उनकी DO की मात्रा को कम कर देता है। DO की मात्रा लवणता बढ़ने पर घटती है तथा दाब के बढ़ने पर बढ़ती है।
- DO (Dissolved Oxygen) : यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिये आवश्यक होती है। जब जल में DO की मात्रा 8.0 mg/लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को संदूषित (Contaminated) कहा जाता है। जब यह मात्रा 4.0 mg/लीटर से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित (Highly Polluted) कहा जाता है।
- BOD (Biological Oxygen Demand) जैविक ऑक्सीजन मांग : ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिये आवश्यक होती है। जहाँ उच्च BOD है वहाँ DO निम्न होगा। जल प्रदूषण की मात्रा को BOD के माध्यम से मापा जाता है। परन्तु BOD के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चलता है साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसलिये BOD को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
- COD (Chemical Oxygen Demand) रासायनिक ऑक्सीजन मांग : जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों (घुलनशील अथवा अघुलनशील) के ऑक्सीकरण के लिये आवश्यक होती है। यह जल प्रदूषण के मापन के लिये बेहतर विकल्प है।
- MPN (Most Probable Number) (सर्वाधिक संभाव्य संख्या ) : जिस जल में जल-मल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसमें ई. कोलाई (E.Coli) जैसे जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। MPN परीक्षण की सहायता से ई. कोलाई आदि जीवों को पहचाना एवं मापा जा सकता है। प्रदूषित जल में उच्च MPN पाया जाता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में फ्लोराइड, जिंक, क्रोमियम, भारी धातुएँ (पारा, यूरेनियम, कैडमियम आदि) को पेयजल प्रदूषण के लिये उत्तरदायी माना है।
- EPA 2010 राष्ट्रीय झील आकलन में भारत की 20 प्रतिशत झीलों में उच्च मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदूषक पाए गए। इससे जलीय पारितंत्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
- जलीय पारितंत्र में सुपोषण, जैव आवर्द्धन आदि प्रक्रिया तेज़ हो जाती है।
- प्रदूषित जल का प्रभाव प्रवाल भित्ति पर भी पड़ता है, इससे प्रवाल विरंजन की घटना में बढ़ोतरी होती है।
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड (Biological Oxygen Demand)
जल प्रदूषण को रोकने के लिए BOD परीक्षण किया जाता हैं। जैसे-जैसे जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती हैं, जल में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती हैं, फलस्वरूप ऑक्सीजन की खपत अधिक होने लगती हैं, अर्थात BOD बढ़ जाती हैं, और जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती हैं। यह जलीय जीवों, मछली आदि के लिए जीवन का संकट उत्पन्न करता हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण CH4, H2S, NH3, जैसे प्रदूषण तत्व उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जल में दुर्गन्ध उत्पन्न हो जाती हैं।
जैविक ऑक्सीजन मांग ऑक्सीजन की वह मात्रा है, जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक होती है। यह परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थो की मात्रा का आकलन करता है। जल जितना ही अधिक प्रदूषित होगा, प्रदूषित पदार्थो के विघटन के लिए उसी अनुपात में अधिक ऑक्सीजन की मांग होगी। स्पष्ट है कि BOD जल प्रदूषण के मानक निर्धारण का महत्वपूर्ण घटक है। सामान्यतः नदियों में BOD का स्तर 10 मिलीग्राम लीटर होना चाहिए। जलीय जीवों के लिए घुलित ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen) अर्थात D.0. की निर्धारित मात्रा का बहुत महत्व है। घुलित ऑक्सीजन से ही जलीय जीव जीवित रहते हैं। जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी होने से जलचरों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। जल जल में प्रदूषण बढ़ता है तो प्रदूषक पदार्थो में फास्फोरस आदि कुछ ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं, जिनकी उपस्थिति के कारण पादप सुपोषण (Eutrophication) बढ़ता है और पादपों तथा कुछ सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, परिणामस्वरूप BOD बढ़ जाती है और जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण मछली जैसे अन्य जलचर मरने लगते है। ऑक्सीजन की कमी से होने वाले अनाक्सी श्वसन के चलते द्वितीयक प्रदूषक जैसे- मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन सल्फाइड आदि बनने लगते हैं जिससे जल में दुर्गन्ध आने लगती है। विदित है कि पेयजल में घुलित ऑक्सीजन 5 मिग्रा/लीटर एवं स्नान के लिए जल में 4 मिग्रा/लीटर निर्धारित की गयी है, कि यदि जल में घुलित ऑक्सीजन का मात्रा 4 मिलीग्राम/लीटर से कम होने पर जल को प्रदूषित कहा जाता है।
मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव (Effects on Human Health)
घरेलू मल जल वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी प्रोटोजोआ तथा अन्य कृमियों जैसे जीवाणुओं को ढोता है। इसलिए संक्रमित जल से होने वाली बीमारियों जैसे पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अमीबी अतिसार के जीवाणु होते हैं। इस तरह का संक्रमित जल पीने, नहाने, तैरने एवं खेती योग्य नहीं होता है। भारी धातु संक्रमित जल से गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। पारा द्वारा जहरीलेपन का शिकार (मिनामाटा बीमारी) जापान की मिनामाटा खाड़ी से Hg संक्रमित मछलियों खाने के कारण हुआ। इसकी जांच 1952 में हुई। पारा मिश्रण में अवशिष्ट जल बैक्टिरिया क्रियाओं द्वारा अत्यधिक जहरीले मिथाइल पारा में बदल जाते है, जिससे अंग होंठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते है, इसके अलावा बहरापन, आंखों का धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन हो जाता है। कैडमियम, प्रदूषण से इटाई-इटाई बीमारी (आउच-आउच बीमारी हड्डियों तथा जोड़ों की दर्दनाक बीमारी) एवं लीवर तथा फेफड़े का कैंसर हो जाता है।
प्रदूषित जल में उपस्थित वायरस, जीवाणुओं, परजीवियों एवं कृमियों के कारण संक्रमण जन्य रोगों, जैसे- पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, हेपेटाइटिस, किडनी खराब आदि का खतरा रहता है। यह संक्रमित जल पीने, नहाने, खाना बनाने आदि के लिये अनुपयुक्त होता है।
भारी धातुओं से युक्त जल के प्रयोग से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। पारायुक्त जल से प्रभावित मछलियों के सेवन से 1956 में जापान में मिनामाटा बीमारी से अनेक लोगों की मौत हो गई थी। अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा मिश्रण सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा अत्यधिक विषैले पदार्थ मिथाइल पारा (Methyl Mercury) में बदल जाता है जिससे अंगों, होंठ, जीभ आदि में संवेदनशून्यता; बहरापन, आँखों का धुंधलापन एवं मानसिक असंतुलन हो जाता है।
कैडमियम प्रदूषण से 'इटाई-इटाई' रोग हो जाता है जिससे हड्डियों एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है तथा यकृत एवं फेफड़े का कैंसर हो जाता है।
सीसा युक्त जल से एनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी एवं मसूड़ों में नीलापन आदि प्रभाव दिखाई देते हैं।
एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल द्वारा एस्बेस्टोसिस (फेफड़े के कैंसर का एक रूप) रोग हो जाता है।
आर्थिक प्रभाव
जल प्रदूषण का आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक दृष्टिगोचर होता है। स्वच्छ पानी (Mineral Water) के मूल्य की तुलना में प्रदूषित पानी को स्वच्छ करना महँगा पड़ता है। जल प्रदूषण से मछलियों व अन्य जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ता है। इसका नकारात्मक प्रभाव पर्यटन पर भी पड़ता के है। एक अनुमान अनुसार, जल प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष $50 बिलियन का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान होता है।
जल प्रदूषण का नियंत्रण (Control of Water Pollution)
जल प्रदूषण को निम्नलिखित उपायों द्वारा प्रभावशाली तरीके से अपनाकर नियंत्रित किया जा सकता है
- प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए।
- शोधन (Purfication) के पूर्व औद्योगिक अपशिष्टों (Industrial Waste Product) को लगाना चाहिए जिससे इनके द्वारा निकला जल शुद्ध होने के बाद जल स्त्रोतों में जा सके।
- समय- समय पर जल स्त्रातों से हानिकारक पौधों को निकाल देना चाहिए।
- लोगों को नदी, तालाब, झील में स्नान नहीं करना चाहिए।
- कीटनाशकों (Insecticide), कवकनाशियों (Fungicides) इत्यादि के रूप में निम्नीकरण योग्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए।
- खतरनाक कीटनाशियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
- पशुओं के प्रयोग के लिए अलग जल स्त्रोत का प्रयोग करना चाहिए।
- ताप तथा परमाणु बिजलीघरों से निकलने वाले जल को ठंडा होने के बाद शुद्ध करके ही जल स्त्रोतों में छोड़ना चाहिए।
- कुछ मछलियां हानिकारक जंतुओं के लार्वा तथा अंडों को खाकर उनकी संख्या को कम करती है। इन्हें जल स्त्रोतों में पालना चाहिए, जैसे-गैम्बुशिया मछली मच्छर के अंडों व लार्वा का भक्षण करती है।
- कृषि कार्य में उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग पर नियंत्रण लगाना चाहिए।
- जल प्रदूषण के दुष्परिणामों से जनमानस को अवगत कराना चाहिए।
- सरकार व समाज मिलकर प्रदूषित जल की स्वच्छता संबंधी अभियान चलायें।
- आणविक विस्फोट से समुद्र को बचाना चाहिए।
- घरेलू सीवेज : घरेलू सीवेज में 99.9% जल एवं 0.1% प्रदूषक होते हैं। शहरी क्षेत्रों के घरेलू सीवेज के 90% से अधिक प्रदूषकों को केंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा हटाया जा सकता है।
- औद्योगिक अपशिष्ट जल : कुछ उद्योगों द्वारा सामान्य विषाक्त प्रदूषकों का उत्सर्जन किया जाता है जिनका निपटान नगरपालिका द्वारा किया जा सकता है किंतु कुछ प्रदूषकों जैसे तेल, ग्रीस, भारी धातुओं आदि का निपटान विशेष निपटान संयंत्रों द्वारा किया जाना चाहिये। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये यह अनिवार्य किया जाना चाहिये कि वे कारखानों से निकले अपशिष्टों को बिना शोधित किये नदियों, झीलों एवं तालाबों में विसर्जित न करें।
- कृषि अपशिष्ट जल : कृषि क्षेत्र में अनेक अपरदन नियंत्रण प्रणालियों द्वारा जल के प्रवाह को कम किया जा सकता है। किसान उर्वरकों एवं कीटनाशकों का आवश्यकता से अधिक उपयोग न कर तथा जैव-उर्वरकों एवं जैव-कीटनाशकों का प्रयोग कर जल की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं।
- आम जनता को जागरूक किया जाना चाहिये एवं जल प्रदूषण एवं उससे उत्पन्न कुप्रभावों से अवगत कराना चाहिये।
- सरकार को जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिये प्रभावी कानून बनाना चाहिये। यद्यपि सरकार ने जल (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 लागू किया था लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
भूमिगत जल प्रदूषण (Ground Water Pollution)
औद्योगिक, नगरीय एवं कृषि अपशिष्टों से युक्त जल के रिसकर भूमिगत जल से मिल जाने से भूमिगत जल संक्रमित हो जाता है। स्वच्छ पानी की कुल मात्रा में भूमिगत जल लगभग 30 प्रतिशत है। भूमिगत जल 1.5 बिलियन लोगों के लिये जल का प्राथमिक स्रोत है। भूमिगत जल में कमी मानव के लिये कृषि समेत अन्य गतिविधियों के लिये विकट समस्या पैदा करती है।
भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल को औद्योगिक तथा नगरीय अपशिष्टों उत्सर्जन सीवेज चैनलों तथा कृषि से बहकर आए जलों से होने वाले क्षरण के कारण संक्रमण का खतरा है। उदाहरण के लिए पेयजल में नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा नवजात शिशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया कर असक्रिय मिथेमोग्लोबीन बनाता है जो कि ऑक्सीजन यातायात को विकृत बना देता है। इसे मिथेमोग्लोबीनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते है। पेयजल में फ्लूराइड की अत्यधिक मात्रा दांतों की विषमताओं को जन्म देती है हड्डी में कड़ापन तथा अकड़न आ जाती है तथा जोड़ों का दर्द होता है (कंकाल फ्लूरोसिस)। भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं खासकर प्रकृति में पाए जाने वाले बेडरॉक के आर्सेनिक से। भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से भूमि तथ चट्टानों के स्रोतों से आर्सेनिक का निक्षालन शुरू हो सकता मत हो सकता है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है। आर्सेनिक से डायरिया, पेरिफेरल न्यूरीटिस तथा हाइपरकेराटोसिस तथा फेफड़े एवं त्वचा का कैंसर हो सकता है।
भूमिगत जल प्रदूषण का प्रभाव (Effects of Ground Water Pollution)
पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से यह नवजात शिशुओं के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मिथेमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। इससे नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को मिथेमोग्लोबीनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है।
पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है जिससे दाँत एवं हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आर्सेनिक युक्त जल के प्रयोग से ब्लैक फुट नामक चर्म रोग हो जाता है। इसके अलावा आर्सेनिक से डायरिया, हाइपरकिरेटोसिस, पेरिफेरल न्यूरीटिस तथा फेफड़े एवं त्वचा का कैंसर हो जाता है।
जल गुणवत्ता को सुधारना (Improving Water Quality)
औद्योगिक तथा नगरीय अपशिष्ट जल को उत्सर्जन उपचार संयंत्र (ETP) में शुद्ध किया जाता है तब इसे जलाशयों में डाला जाता है। साधारणत: निम्नलिखित उपचार किए जाते है।
- प्राथमिक उपचार : इस भौतिक प्रक्रिया में जल के मलबों से अलग कर उसे टैंक में छोड़ दिया जाता है, जिससे तलछटों में गंदगी जम जाए।
- द्वितीयक उपचार : यह एक जैविक प्रक्रिया है तथा यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा कराया जाता है। इस उपचार में, अवशिष्ट जल को उथले टैंक में स्थायीकरण के लिए डाला जाता है। जहां कार्बनिक पदार्थो का ऑक्सीकरण जीवाणुओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में CO2 का निष्कासन होता है तथा जैव ठोस का निर्माण होता है। जैव ठोस लगातार वातित होकर ऑक्सीकरण करता है। शैवालों का अपशिष्ट जल के ऊपरी प्रकाशित भाग में विकास होने से O2 का उत्पादन होता है जिससे वातन होता है।
- तृतीयक उपचार : इस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया में पोषण की उपस्थिति के कारण (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इत्यादि)-घुले हुए कार्बनिक पदार्थ, धातु या रोगाणु को हटाया जाता है। इस चरण में अपशिष्ट जलों का मजबूत ऑक्सीकारकों जैसे क्लोरीन गैस परक्लोरेट नमक, ओजोन गैस तथा UV विकिरण द्वारा रासायनिक ऑक्सीकरण हो जाता है। तीसरे उपचार के बाद अपशिष्ट जल को प्राकृतिक जलाशयों में छोड़ा जा सकता है या कृषि के लिए उपयोग किया जा सकता है।
जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये सरकारी प्रयास
- जल स्त्रोतों के प्रदूषण स्तर का सर्वेक्षण।
- औद्योगिक स्त्राव के निष्कासन का परीक्षण तथा उस पर निगरानी।
- प्रदूषित जल के शोषण के उपायों की खोज।
- स्थानीय निकायों को जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुझाव देना।
- प्रदूषण के प्रति आम जनता में जागरूकता पैदा करना।
जल निकायों का संरक्षण (Conservation of Water Bodies)
भारत की अधिकतर नदियाँ इस समय प्रदूषित नालों के समान बन गई हैं। भारत के आधे तालाब, झील प्रदूषण के शिकार हैं तथा इनका जल पीने योग्य नहीं रह गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय' का कार्य केन्द्र प्रायोजित स्कीमों 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP)' एवं 'जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना' (NPCA) के तहत नदियों, झीलों एवं नम भूमियों के संरक्षण के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
गंगा एक्शन प्लान (GAP)
देश की प्रमुख नदियों में से एक तथा स्वयं का निर्मलीकरण (गंगा में पाए जाने वाले वाइरस जैसे Bacteriophage वगैरह जीवाणु आदि को खा जाते हैं।) करने वाली गंगा आज लगभग अपने अपवाह के आधे भाग में प्रदूषित हो गई है। वर्तमान में 50,000 से अधिक आबादी वाले 100 से अधिक शहरों का असंसाधित मल-अपशिष्ट गंगा में अपवाहित किया जाता है तथा हज़ारों की संख्या में लाशों व जले हुए अवशेषों को इसमें प्रवाहित किया जाता है। गंगा बेसिन में भारत की लगभग 35 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 'केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण' (CGA) का गठन कर 1985 में गंगा एक्शन प्लान (GAP) की शुरुआत की गई। GAP-I सन् 1986 से 1993 तक चला।
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (National River Conservation Plan)
1995 में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण (CGA) का नाम बदलकर 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण' (NRCA) कर दिया गया था। गंगा कार्ययोजना का विलय NRCP के साथ कर दिया गया। वर्तमान में इसमें 19 राज्यों में फैले 121 शहरों की 40 नदियों के प्रदूषित भाग को शामिल किया गया है।
- NRCP का उद्देश्य प्रदूषित नदियों के किनारे बसे विभिन्न शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्यों के ज़रिये नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- NRC के तहत किये गए प्रदूषण उपशमन कार्यों में खुले नालों से नदियों में आ रहे कचरे को रोकने के लिये मल व्यवस्था प्रणाली बनाना, गंदे जल के शोधन के लिये जल शोधन संयंत्र लगाना, नदी किनारे शौच पर प्रतिबंध, नदी तट एवं स्नान घाटों का सुधार, सहभागिता, जागरुकता इत्यादि शामिल हैं।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला (ERL) लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के परीक्षणोपरांत जल को पांच श्रेणियों में विभक्त किया है-
- वर्ग A (Category A) - पीने के लिये उपयुक्त
- वर्ग B (Category B) - स्नान, तैराकी और मनोरंजन के लिये उपयुक्त
- वर्ग C (Category C) - पारम्परिक उपचार के बाद पीने योग्य
- वर्ग D (Category D) - वन्यजीव और मछलियों के लिये उपयुक्त
- वर्ग E (Category E) - सिंचाई, औद्योगिक शीतलन और अपशिष्ट निपटान हेतु उपयुक्त
| क्र.सं. | नदी | क्र.सं. | नदी |
|---|---|---|---|
| 1. | अडयार | 21. | महानंदा |
| 2. | बेतवा | 22. | मिंद्यौला |
| 3. | ब्यास | 23. | मूसी |
| 4. | बीहर | 24. | नर्मदा |
| 5. | भद्रा | 25. | पेन्नार |
| 6. | ब्राह्मणी | 26. | पंबा |
| 7. | कावेरी | 27. | पंच गंगा |
| 8. | कूम | 28. | रानी चियू |
| 9. | चंबल | 29. | साबरमती |
| 10. | दामोदर | 30. | सतलज |
| 11. | दीफू और धनश्री | 31. | स्वर्णरेखा |
| 12. | घग्गर | 32. | ताप्ती |
| 13. | गोदावरी | 33. | तापी |
| 14. | गोमती | 34. | तुंगा |
| 15. | खान | 35. | तुंगभद्रा |
| 16. | कृष्णा | 36. | ताम्रबरनी |
| 17. | क्षिप्रा | 37. | वैगाई |
| 18. | महानदी | 38. | वैन्नार |
| 19. | मंदाकिनी | 39. | वेनगंगा |
| 20. | मांडवी | 40. | यमुना |
जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय योजना (National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem : NPCA)
झीलों एवं नम भूमियों के संरक्षण के लिये पूर्व में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा था-
- राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना
दोहराव से बचने एवं बेहतर समन्वय के लिये इन दोनों योजनाओं को एकीकृत कर NPCA आरंभ की गई। योजना की लागत को केन्द्र व राज्य सरकारों में क्रमश: 70:30 के अनुपात में तथा विशेष राज्यों के मामले में 90:10 में बाँटा गया। इस योजना का लक्ष्य जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये झीलों एवं नम भूमियों का संरक्षण एवं पुनरुद्धार तथा एक सामान्य विनियामक संरचना के माध्यम से जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी में सुधार लाना है। यह योजना झीलों के प्रदूषण में कमी लाएगी एवं नम भूमि संसाधनों के तर्कसंगत इस्तेमाल में सहायता प्रदान करेगी।
विश्व में लगभग 15 करोड़ लोग आर्सेनिक युक्त जल पीने को मजबूर हैं। भारत में 10 राज्यों में आर्सेनिक प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। आर्सेनिक की 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।
जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम 1974
यह अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये बनाया गया है। इसके माध्यम से विभिन्न बोर्डों का गठन किया गया है, जो जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करते हैं। अधिनियम द्वारा बोर्डों को अधिकार एवं कर्त्तव्य प्रदत्त किये गए हैं।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य निम्नलिखित हैं-
- केंद्र सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना।
- राज्य बोर्डों के कार्यों का एकीकरण।
- राज्य बोर्डों को जल प्रदूषण जाँच और शोध-कार्य में सहायता प्रदान करना।
- जल प्रदूषण विशेषज्ञों की ट्रेनिंग।
- जल प्रदूषण संबंधी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा जनसाधारण को प्रदान करना।
- संबंधित तकनीकी व सांख्यिकी सूचना को एकत्र, एकीकृत एवं प्रकाशित करना।,,
- सरकार की सहायता से जल प्रदूषकों का मानक तय करना तथा समय-समय पर उन्हें पुनरीक्षित करना।
- जल प्रदूषण रोकने के लिये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य राज्य सरकार के जल प्रदूषण रोकने के कार्यक्रम का संचालन।
- राज्य सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना।
- राज्य स्तर पर जल प्रदूषण संबंधी सूचनाएँ एकत्र करना एवं उन्हें प्रकाशित करना।
- जल प्रदूषण रोकने के लिये अनुसंधान कराना।
- विशेषज्ञों की ट्रेनिंग में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करना।
- सीवेज तथा उत्स्गों का उपचार की दृष्टि से निरीक्षण करना।
- जल प्रदूषण के मानक स्थापित एवं पुनरीक्षित करना।
- जल उपचार के कारगर व सस्ते तरीके निकालना।
- सीवेज तथा उत्सर्ग के उपयोग-प्रयोग ज्ञात करना, सीवेज एवं उत्सर्ग हटाने के उचित तरीके निकालना।
- उपचार के मानक स्थापित करना, सरकार को उन उद्योगों की जानकारी देना, जो हानिकारक उत्सर्ग बाहर छोड़ रहे हों।
- बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी उद्योग से उत्सर्जित जल का नमूना ले सकते हैं। बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी उद्योग का निरीक्षण कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को जानबूझकर कोई विषाक्त, नशीला पदार्थ किसी जल धारा में निर्गत करने का अधिकार नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने पर तीन माह की कैद या जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान है। कंपनियों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।
नमामि गंगे कार्यक्रम
केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में नमामि गंगे नामक फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिये 20,000 करोड़ आवंटित किये गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण जीर्णोद्धार एवं प्रदूषण को खत्म करना है।
नमामि गंगे कार्यक्रम के निम्नलिखित मुख्य स्तंभ हैं-